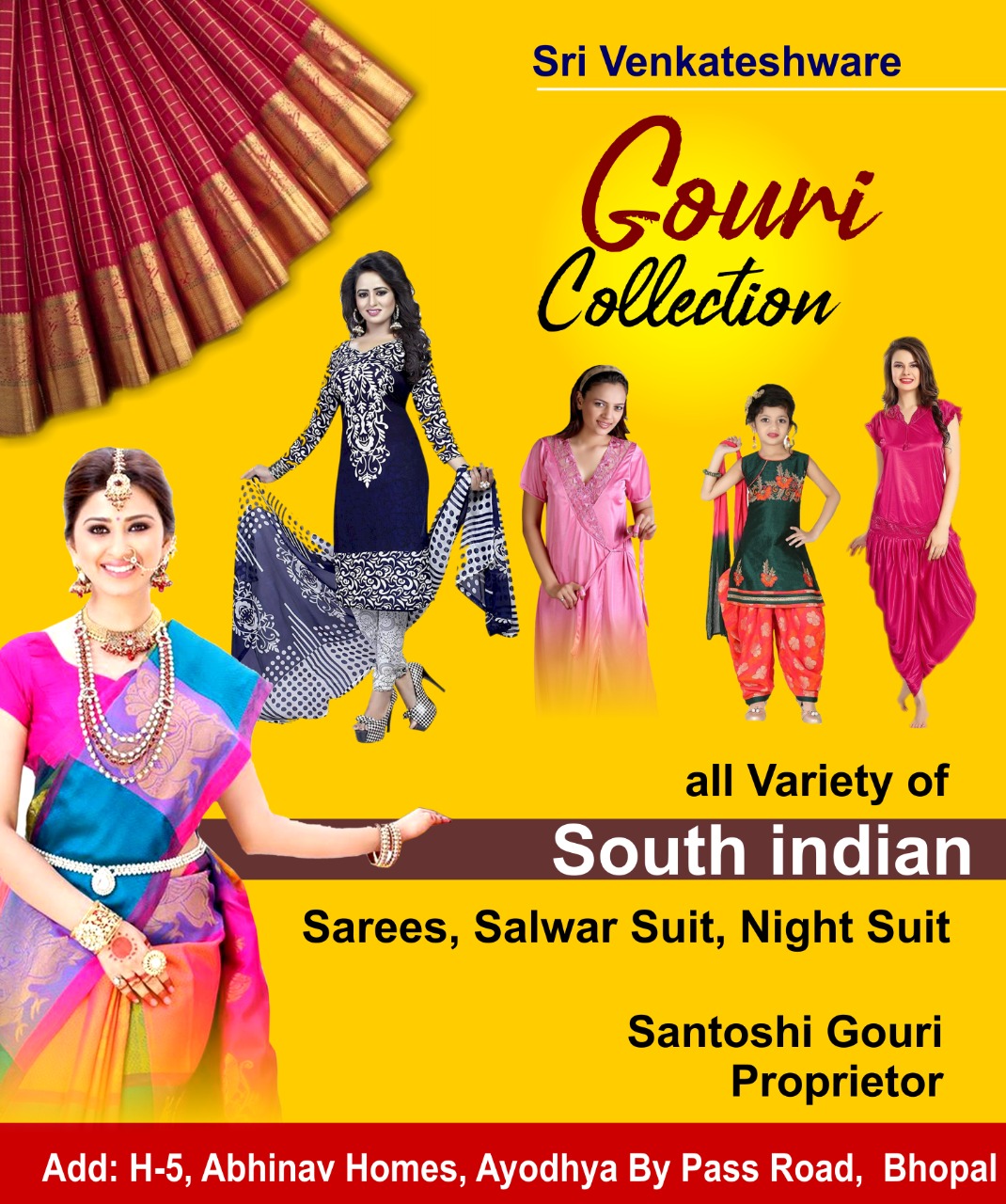मुंशी प्रेमचन्द जन्म-31-07-1880 - जयंती-31-07-2025

मुंशी प्रेमचन्द जन्म-31-07-1880 - जयंती-31-07-2025
‘प्रेमचंद जी के साहित्य में विद्धमान भारत को खोजा जाए’
(प्रेमचंद जी के उपन्यासों एवं कहानियों की वर्तमान व भविष्य में प्रासंगिकता व उपादेयता.।)
“ प्रेमचंद के लिए भारतीयता भारतीय मनुष्य की अस्मिता, जिजीविषा,उदात्तता और श्रेष्ठता उनका प्रतीक था। उन्होंने अधम, अपराधी तथा अत्यंत साधारण मनुष्य में मानवीय भावों को स्पंदित करके भारतीयता की श्रेष्ठता को सिध्द कर दिया ।”
हिंदी साहित्य के विषय में जब भी बात चलती है तो हमारे वरिष्ठ हमेशा यह कहते है, हिन्दी साहित्य जगत में जिसने प्रेमचंद नहीं पढ़ा, उसने हिन्दुस्तान नहीं पढा ...उपन्यास सम्राट प्रेमचंद ।
उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के समीप लमहीं गाँव में हुआ। मात्र पाँच वर्ष की उम्र में माता का देहान्त। पिता डाकखाने मे मुलाजिम थे आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी जिसके कारण उनकी पढाई में भी बाधा रही। पिता के स्थानान्तरण के कारण नई जगहों का अनुभव उन्हें बहुत मिला, 14 वर्ष की छोटी उम्र मे विवाह हुआ बताया जाता है उनकी पत्नी के साथ कभी नहीं बनी पत्नी ने उन्हें छोड कर अपने मायके चली गई फिर उनकी विवाह एक बालविधवा शिवरानी से हो गया।
प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व में देशभक्ति का जज्बा तथा कृतित्व में राष्ट्रीयता का गहरा रंग सहज ही परिलक्षित होता है । उन्होंने एक सच्चे साहित्यकार के साथ-साथ एक जिम्मेदार नागरिक का भी दायित्व बखूबी निभाया है ।जिसके कारण वे आज भी अनुकरणीय हैं , समकालीन लेखकों के लिए भी प्रासंगिक है और आदर्श भी। प्रतिकूल परिस्थितियों में जन्में साहित्य के ऐसे नक्षत्र रहे मुंशी प्रेमचंद जी का साहित्य भारतीय समाज का ऐसा आईना है जिसमें दशको पहले की गरीबी,शोषण,वर्ग-वाद और समाज के ठेकेदारों की जो तस्वीर दिखाई देती है, वर्तमान में भी लगभग वही है। इसी कारण इनका साहित्य कालजयी हो गया है। वे गरीबी के कारण शोषण के शिकार बचपन से ही थे। भारतीय कथा-साहित्य पर उनकी छाप बहुत गहरी है। ऐसी समृध्द विरासत में आलोचकीय मुल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया के सतत चलते रहने के परिणाम ही है,जो हमें हमेशा आज के दिन उनकी जयंती पर बार-बार उनके कृतित्व पर एक चर्चा के लिए बैठने को मजबूर करती है। मुंशी प्रेमचंद जी की साहित्यिक व्यापकता के कारण उनके साहित्य की समीक्षा-आलोचना –शोध का इतिहास भी व्यापक है। एक विधा उपन्यास से पहले आख्यान–जो फिर उपन्यास का स्वरूप बना। गोदान के पात्र होरी के शब्द –“जब गर्दन पाँवों के नीचे दबी हो तो पाँव सहलाने में ही भलाई है।“ (किसान की दुर्दशा, कमजोर स्थिति प्रतिरोध को कुचल देने का भय। बलशाली की चापलूसी में ही भलाई है।) जिससे दबी ही सही उसकी अस्मिता बची रहे। किसान की आज भी हमारी कामाबेश यही स्थिति है। कथा सम्राट प्रेमचंद के जीवन के साहित्यिक आयाम के कई पहलू रहे। कहानियों का विपुल भंडार, उपन्यासों से समाज, राष्ट्रीयता, किसानों मजदूरों की समस्याएं, नारी जीवन की त्रासदी के कई स्वरूपों का वर्णन मिलता है

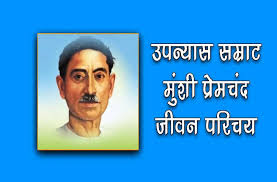


नाटक,समीक्षा,आलोचना का भी दौर रहा । इनकी तुलना –रूसी के लेखक मेक्सिम–गौर्की से व चीन के लेखक ल्यूयेन से करते है ।
ऐसा भी माना गया है की 1857 की लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ़ मात्र सैनिकों की नहीं वर्ना किसानों की लडा़ई भी थी –जिसे बड़ी निर्ममता के साथ कुचला गया। इनकी मनोमस्तिष्क पर अंग्रेजी सरकार की क्रूरता से लगान के कानून का एक किसान होने के उसका सीधा प्रभाव उनके उपन्यासों मे भी रहा ,वह दिन प्रतिदिन गहराता गया । इस तरह के शोषण का शिकार किसान जमींदारों व महाजनों की साँठगाँठ के साथ लगातार शोषित हो रहा था । इसके परिणाम व अन्य कई कारणों से किसान का जीवन दूभर होता गया। पहले ही अंग्रेजी सरकार की औद्योगीकरण की नीति के कारण त्रस्त रहा किसान। पहले किसानों की खेती , शिल्पकारी व दस्तकारी से धीरे धीरे बेदखल होते रहे। जो किसान को किसानी से मजदूर बनाने के लिए मजबूर होने के क्रम का सूत्रपात था । इस प्रकार किसी भी प्रकार के सुधार के प्रयास में उठाई गई आवाज राजनीतिक या नवजागरण के नेताओं व्दारा –मात्र एक प्रर्थना पत्र तक ही सीमित रह जाती थी। फिर अंग्रेजी शासन के अत्याचार का आरंभ हुआ एक नया दौर –नील की खेती, मादक पदार्थों की खेती (अफीम) आदि.। चम्पारण का सत्याग्रह, बारदौली के सत्याग्रह, रायबरेली और प्रतापगढ के आंदोलन—जो हमेशा याद किए जाते है। इसके बाद एक बहुत ही दर्दनाक घटना1919 का जलियांवाला बाग काण्ड, जिसने भारत के अंदर आजादी का ऐसा बिगुल बजा दिया जिसने अंग्रेजों की रातो की नींद दिन का चैन हराम कर दिया इनके विरूध अब ऐसा असर हो गया की क्रांतिकारी दलों का आगमन हो गया ।उसके बाद 1920 के चौराचौरी घटना से भारतीयों मे निराशा का संचार होने लगा । इस समय प्रेमचंद जी गाँधी जी से प्रभावित थे ,परंतु गाँधी जी ने प्रेमचंद के किसानों की दशा को महत्व न देते हुए,स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्राथमिकता से जुट गये और ये कहा पहले इसे प्राप्त कर लें फिर किसानों के बारे में सोचेगें। तब प्रेमचंद जी ने कहा था कि ,मैं गाँधी का सम्मान करता हूँ, पर मुझे किसानों के बारे में भी सोचना है। प्रेमचंद जी का मार्क्सवाद की ओर झुकाव हुआ, रूसी क्रांति1917 (क्रांतिकारी लेनिन) में जो हुई थी उससे परिणामों के नतीजे के परिपेक्ष्य में हम देख सकते है। इस क्रांति के बाद जो लेखनी का अलग प्रभाव मिलता है किसानों के मजदूर बनने तक की यात्रा। आज हमारे पास प्रेमचंद जी के बारे में कहने को जिस प्रकार बहुत कुछ है, उसी प्रकार हमें उनकी तरह कुछ करने में भी सक्षम हो सके तो ही इसकी सार्थकता आने वाले समय में हमे मिलेगी। कथनी –करनी के अंतर को कम करना जरूरी है 145 वें वर्ष की इस जयंती को यादगार बनाना है तो इसे उनके विचारों को अपने जीवन मे दृढ़ता से पालन भी करना जरूरी।
उनके व्दारा देश की सामाजिक,आर्थिक,राष्ट्रीयता के लिए जो मापदण्ड रहे व किसानों,मजदूरों,मध्यम वर्गीय संघर्ष, महिलाओं के बारे में जो वैचारिक खाका बनाया उसके अनुकूल वर्तमान समय के आकंलन से अगर हम गुजरते है, तो लगता है हम जहाँ थे वहीं है । अर्थात शोषण जारी है,किसान बदहाल है,पूंजीपतियों का बोलबाला है ,नारी अत्याचार के नये नये तरीके ईजाद हो गये, राष्ट्र की राजनीति को उसके मूल तत्वों को दीमक ने चाट लिया है । किसान आत्महत्याएँ कर रहा है, आज भी किसान अपनी उचित स्थिति को पाने के लिए आंदोलन कर रहा है –हमारा देश ‘’अमृतमहोत्सव’’ आजादी की 75वीं वर्षगाँठ भी हमनें मना ली है और 80 वें व्रर्ष के करीब आ पहुँचे है।
उपन्यास के विकास क्रम को चार हिस्सों में बाँटा जा सकता है-
(1.) प्रेमचंद पूर्व युग का उपन्यास साहित्य (2.) प्रेमचंद युग का उपन्यास साहित्य
(3.) प्रेमचंदोत्तर युग का उपन्यास साहित्य (क)मनोवैज्ञानिक उपन्यास—-शेखर एक जीवनी,(ख),सांस्कृतिक ऐतिहासिक उपन्यास—वैशाली की नगर वधू,,वयं रक्षामः,,(ग)सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास—पतन ,चित्रलेखा,,प्रगतिवादी उपन्यास—कामरेड,,(घ)मेरी तेरी उसकी बात,..आँचलिक उपन्यास—मैला आंचल, अंधा गाँव.।
(4) स्वातंत्रोर समकालीन उपन्यास साहित्य—स्वतंत्रता के बाद की परिस्थितियों का असर – प्रयोगवादी उपन्यास या आधुनिकता बोध के उपन्यास कहा जा सकता है। औधयोगीकरण, भ्रष्ठ-व्यवस्था, बदलते परिवेश, यांत्रिक सभ्यता के दुष्परिणाम, महानगिरीय जीवन, अकेलापन, निराशा, धोर अवसाद, तनाव आदि विषयों के साथ उपन्यास की वस्तु और प्रक्रिया नवीन होती गई। स्वतंत्रता के बाद कई तरह की नई चुनौतियाँ भी आयी ।
उपन्यास का आगमन–
(1) उर्दू उपन्यास 1903से—1905)-असरारे मआविद(देवस्थान रहस्य)(2)-हमखुर्मा-ओ-हमसवाब(1906)-हिंदी अनुवाद प्रेमा—1907 । (3)-जल्वा-ए-ईसार(1912)-हिंदी अनुवाद वरदान 1921 में । (4)पहला बड़ा उपन्यास सेवासदन—(उर्दू में बाजारे-हुस्न)-।(प्रेरणा—मिर्जा हादी रूसवा के उपन्यास(उमराव जान अदा-1899) से व इसी तरह किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास –स्वर्गीय कुसुम भी इससे समानता रखती है)(5)-प्रेमाश्रम-1922 (6)-रंगभूमि-1925(7) काया कल्प(8)-कर्मभूमि (9)-गोदान (10)- निर्मला (11)-गबन-(12)-सूरदास(13)-रामचर्चा(14)-बरदान(15)-दुर्गादास(16)-अंलकार(17)-प्रतिज्ञा(मंगलसूत्र)
इनके उपन्यासो की विशेषताएँ- (1)-यथार्थ वादी दृष्टिकोण(2)-ईश्वर के प्रति अनास्था का भाव.—भाग्यवाद की जगह कर्मवाद को महत्व दिया। (3) नैतिक शिक्षा की ओर (4)-नारी के प्रति सहानुभूति(5)-वर्ग संघर्ष की पीड़ा (6))-अंधविश्वासों का विरोध।
प्रेमचंद के उपन्यास आदर्श से यथार्थ की यात्रा का व्याख्यान करते हैं।सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का चित्रण ग्रामीणों का शोषण , जातिगत कुत्सिकता , लैंगिक असमानता , बेमेल विवाह और उससे उत्पन्न समस्याएं आदि ऐसे यथार्थ हैं जो वास्तव में उस समय थे और उन्हीं का प्रकटीकरण प्रेमचंद ने किया है। भाषा इनकी सरल और सहज है , वे भारी भरकम शब्दों से बचते हैं ।
प्रेमचन्द के उपन्यास अपने समय की यथार्थ तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, यद्यपि प्रेमचंद के उपन्यासों में आदर्श भी महसूस किया जा सकता है। प्रेमचंद जी के साहित्य की एक और महत्वपर्ण विशेषता यह है कि उन्होंने वही लिखा है जो उन्होंने देखा और भोगा है, यही कारण है कि प्रेमचंद जी और उनका साहित्य विशेष रूप से उनके उपन्यास आज भी प्रासंगिक हैं। प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यासों में अपने समय के समाज को बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत किया है ।उनके उपन्यासों में किसानों के दर्द, स्त्रियों की स्थिति आदि का बहुत ही संजीदगीपूर्ण वर्णन किया गया है।उनके उपन्यासों को पढ़ते समय आप स्वयं उस दर्द को महसूस करते हैं।
मुंशी प्रेमचंद के समय अय्यारी और तिलस्मी साहित्य का उर्दू में भरमार था। जिसमें प्रमुख देवकीनंदन खत्री –व उनके उपन्यास बहुत ही लोकप्रिय थे। फिर इनके उपन्यास का दौर आरंम्भ हुआ पहले इन्होंने भी उर्दू में पहला उपन्यास लिखा उर्दू उपन्यास असरारे मआविद (देवस्थान रहस्य) जिसे अधूरा माना गया। इनकी लेखनी ने अय्यारी व तिलिस्म को नहीं चुना—एक अलग ही क्षेत्र का चयन किया। इसी के कारण इन्हें एक अलग पहचान मिली है। भारतभूमि से जुडे यथार्थ पात्रों को अपने उपन्यासों में प्रधानता के साथ स्थान दिया। गली-कूँचों को एवं गाँवों को इसका मंच बनाया..एक अलग और मौलिक प्रयोग था। आरम्भिक उपन्यासों में सामाजिक प्रसंगों –समस्याओं यथा—धार्मिक आडम्बर,विधवा-विवाह, वेश्यावृति आदि –मूल में रहे। असरारे मआविद (देवस्थान रहस्य)जिसे अधूरा माना गया।—इसमें तीर्थ स्थलो,मंदिरों में व्याप्त भ्रष्टाचार, वेश्यावृति एवं स्त्रियों के त्रियाचरित्र का उदघाटन किया। उदेश्य केवल देश में व्याप्त जाति-पात, भेद-भाव के आचरण को समाप्त करना चाहते थे। आदि इन बुराईयों को समाप्त करने के प्रयास कर रहे थे। पर आज भी उसकी जडें मौजूद है। शहरो में जरूर कुछ कम है पर गाँवों में अभी भी इसका निर्विवाद भारत में विधामान है।
दूसरा उपन्यास—भी उर्दू में “ हमखुर्दा-ओ-हमसवाब’’(1906) पर(इसमें विधवा विवाह मुख्य मुद्दा था) इसका हिंदी अनुवाद स्वयं प्रेमचंद जी ने किया था ‘’प्रेमा’’(1907) (दो सखियों का विवाह) इसी क्रम में इन्होंने तीसरा उपन्यास ‘’जलवा-ऐ-ईसार’’(1912) लिखा इसका भी हिंदी अनुवाद ‘’वरदान’’ (1921) में नाम से लिखा गया ।
यह क्रम यहाँ से समाप्त नहीं होता इनके कई बहुत ही बड़े रूप में लिखे हिंदी उपन्यास ‘’सेवासदन’’ की पृष्ठभूमि भी उनके उर्दू में लिखे ‘’बाजारे हुस्न’’ नाम से लिखा गया था। इस उपन्यास के माध्यम से प्रेमचंद जी ने हिंदी उपन्यास के क्षेत्र में अपने कदम स्थापित किए। इस उपन्यास की प्रमुखता में वेश्यावृति की समस्या को उठाया । इस उपन्यास को लिखते समय उनके सामने उनकी प्रेरणा के रूप में (उमराव जान अदा-1899 में) लिखी ‘’हादी रूस्वा’’ के उर्दू उपन्यास और किशोरी लाल गोस्वामी के उपन्यास ‘’स्वर्गीय कुसुम’’से बहुत अधिक समानता दिखाई देती है। इस समानता की समस्या को प्रेमचंद ने उक्त दोनों उपन्यासों की तुलना मे एक अलग दृष्टि से निराकरण दिया—‘’सेवासदन’ उपन्यास में वेश्यावृति अपनाये जाने के कारणों को रेखांकित किया गया है। इन कारणों में दहेज प्रथा, पति व्दारा क्रूर व्यवहार, समाज में स्त्री की उपेक्षा और असहानुभूति ऴ इसके साथ समाज मे आर्थिक समस्या व अन्य कारणों को प्रमुख माना। सेवासदन(कार्य व्यापार की प्रधानता थी) इसके पहले हिंदी उपन्यासों में- घटनाओं की प्रमुखता होती थी। साथ ही साथ नारी सौंदर्य ,विरह ,मिलन ,नीतिपरक उपदेश, धर्म, प्रकृति आदि प्रमुख विषय रहते थे। सेवासदन ने कार्य व्यापार की प्रधानता के साथ प्रेरक भावनाओं से संबध के कारण निहित भावनाएँ ही पाठक के कौतुहल व जिज्ञासा का कारण बनी।
इसके बाद एक नयी परिपाटी का उदय हुआ। किस्सागोई और नाटकीयता,कथाओं का यौगिक पदिक क्रमण और उनमें तर्कसंगत संबंध के दर्शन –सेवासदन मे भी होते हैं। प्रिय पाठको वाला संबोधन नहीं रहा ।
दूसरा उपन्यास-हमखुर्दा-ओ-हमसवाब-में कुछ सहज और स्वाभाविक गद्य में लेखन की कलम चली ।
सेवासदन –में संस्कृत गधकाव्य परंपरा की शोभा का कोई चिन्ह नहीं दिखता ।
इसके पहले के उपन्यास ‘’प्रेमा’’ में देवकीनंदन खत्री की उपन्यास की भाषा के करीब –दिखाई देती है । आगे इन्हीं की भाषा को सुधार कर उसे एक नवीन औपन्यासिक भाषा मे प्रस्तुत किया ।
सेवासदन की सफलता का असर उनके बाद के उपन्यासों में–‘प्रेमाश्रम’(1922)—ब्रिटिश राज में जमींदारों, पुलिस और सरकारी अधिकारियों व्दारा किसानों के शोषण का—चित्रण। इनके अन्तर्संबंधों को उद्घाटित किया है। भारत उस समय गुलाम था। ब्रिटिश केवल अपने अधीनस्थ उपनिवेश का आर्धिक दोहन/शोषण कोई कसर नहीं रखी, जिसमें किसान व मजदूर पूरी तरह से अत्यंत ही कष्ट में थे ।
इसी समय के अन्य उपन्यासकारों के उपन्यास में परतंत्रता की सुगबुगाहट नहीं मिलती –वे तो ब्रिटिश शासन का गुणगान ही करती दिखी। परंतु जब ब्रिटिश शासन के दोहरे आचरण का पता चल गया कुछ भी बोलने से परहेज करने लगे ।
इसका साहस प्रेमचंद ने खुद मे पैदा किया –प्रेमाश्रम के बाद रंगभूमि में इसका पुट मिलता है ।इस प्रकार स्वतंत्रता संग्राम का सीधा वर्णन न के बराबर है परंतु भावनाओं को दबा कर नहीं रखा..।
उपन्यास के कुछ पात्र जिनके माध्यम से मध्यवर्गीय परंपरागत रूढिवादी दृष्टिकोण पर आधात पहुंचाया व उनके अन्तर्विरोधों को उकेरा ।
सेवासदन—कृष्णचंद्र—ईमानदार दरोगा। बेटी के विवाह—रिश्वत-फिर मुकदमा। निर्मला- आमदनी से अधिक खर्च का व झूठी शानो-शौकत के कारण निर्मला का विवाह तोताराम एक अधेड़ से करना। इस विवाह से इसका अंत नहीं होता । उसके अलावा और भी मध्यमवर्गीय तोताराम की नैतिक मूल्यों से उपजी समस्याएँ ।
गबन में झूठी चमक-दमक का और भी मार्मिक चित्र उभर कर आया। जालपा के आभूषणों का मोह रामनाथ को हमेशा आत्मग्लानि से भरा रखता ।और गबन करने को मजबूर हो जाता है । (किसान व मध्यवर्गीय समस्याओं को बहुत ही सुंदर तरीके से उकेरा है)
इनके उपन्यासों के स्त्री पक्ष के बगैर तो बात अधूरी ही रह जाएगी , जो समाज और परिवार के केन्द्र में होती है। प्रेमचंद के दौर में नारी की स्थिति में सुधार पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। पहले परंपरागत दायरे में ही सब रहा-आदर्श के रूप में रखा।
प्रेमचंद ने इन वौचारिक सिध्दांतो को मूर्तरूप देने के लिए 1906 में एक बाल विधवा—शिवरानी से विवाह किया। जो मिसाल बनी—फिर उनके ही एक और उपन्यास गोदान में सिलिया और मातादीन के विवाह ने—अन्तर्जाती विवाह के मार्ग बनाए । आधुनिक विचारों के प्रति भी स्थान रखना इनके उपन्यास के अंग रहे।
फिर गाँधी जी के संपर्क में आने के साथ नारी पात्रों की देश सेवा और समाज सेवा की भावना स्वयं उनकी पत्नी शिवरानी का जेल जाना। शराब की दुकान, विदेशी सामान की दुकान धरना। करेला ऊपर से नीम चढा—हमारे यहाँ के पूंजीपति और जमींदार लोग भी इनके पक्षधर बनने लगे ।
एकता विरोधी –नीतियों के तहत हिंदु-मुस्लिम के मध्य साम्प्रदायिक दंगो ने रूप ले लिया—जो 1920 के पश्चात अनेक जगहो पर देखने को मिला। इन कटु सच्चाई को अपने उपन्यासों में ‘’कायाकल्प’’ में चित्रण किया । मानवता के प्रबल समर्थक—पात्र—साम्प्रदायिकता से मुक्त होते थे। पात्र –चक्रधर-इसका धोतक और ख्वाजा महमूद अपने हिंदू मित्र की पूत्री के खातिर अपने बेटे को भी सजा देता है।
जहाँ प्रेमचंद—इसके पक्षधर नही है परंतु –इसकी तह तक पहुँचकर इन दंगों को कराने वाले स्वार्थी लोगों को उजागर करते है । आरोप—यथार्थवादी समस्याओं का समाधान आदर्शवादी एवं कृत्रिम देते है
जो कुछ हद तक सही प्रतीत होता है—उपन्यास –सेवासदन और प्रेमाश्रम—का समाधान आदर्शवादी ही है। शायद यह उस युग की आवश्यकता ही रही -अर्थात कोई अन्य विकल्प था ही नहीं, औपनिवेशिक शासन के चलते। जमींदार, पूंजीपति, महाजन और शिक्षित वर्ग भी –उनकी मशीन के कल-पूर्जे ही बने रहने की मजबूरी थी ।
इसी समय महात्मा गाँधी जी भी समाधान खोज रहे थे—कभी सत्याग्रह, कभी हृदयपरिवर्तन कभी सदकार्यों की स्थापना के लिए आश्रम की व्यवस्था करते। प्रेमचंद भी इसी युग-यथार्थ में जी रहे थे ।
लेकिन गोदान उपन्यास तक आते आते –परिवर्तन आया। किसानों की संगठित आंदोलन—को कथा-वस्तु बनाया। सभी वर्ग के पात्रों को अपने उपन्यास में जगह दी । गरीब-अमीर सभी। उपन्यासों के लिए ताना-बाना परंपरागत आधार पर नहीं बुना,बल्कि वे अपने नियम स्वयं बनाते है।
नायकविहिन—प्रेमाश्रम…सूरदास—का नायक-अंधा भिखारी ‘सूरदास’ बनकर उभरता है। जो अनपढ-गंवार है, जिसमें परंपरागत नायक की छवि ढूंढपाना अपने को हँसी का पात्र बनाना होगा। गोदान का होरी साधारण—उस समय के नायको की परंपरा को इन्होंने तोडा ।
उन्होने उपन्यास की पहले की परिपाटी का अनुस्ररण नहीं किया ,विविधता के साथ आये ..पाठको को संबोधन की शैली का परित्याग किया ..वे उपन्यास में रहते जरूर परंतु अप्रत्यक्ष रूप से । वर्णनकर्ता, सलाहकार एवं किस्सागोई के रूप में यह एक सुंदर प्रयोग था परंतु जो इनके उपन्यास को कभी कभी शिथिलता प्रदान करती थी ।अपने पाठकों को हे बंधु, साथियों आदि संबोधन नहीं किया। पाठक को ऐसा प्रतीत होता है की वह पढ़ नहीं रहा वरन देख रहा है। सारे घटनाक्रम चित्र के स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं यह विशेषता भी रही। टालस्टाय का उपन्यास साहित्य इसका उदाहरण है। इसका प्रयोग प्रेमचंद ने आरंभ कर दिया था। प्रेमचंद के उपन्यासों मे सुगठित कथानक की बाध्यता नहीं थी, क्योंकि वे अपने उपन्यासों में समग्रतापूर्ण विवरण प्रस्तुत करते थे। मात्र मंनोरंजन या कोरे उपदेश के लिए न होकर उसमें यथार्थ लिए विविध रंग होते थे ।
प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि और गोदान –में स्पष्ट प्रभाव के प्रमाण मिलते है। इनके उपन्यास गोदान में—कहीं पर भी नगर व गाँव को जोड़ने का प्रयास के प्रतीक नहीं मिलते। साहित्य में प्रेमचंद के महत्व को स्वीकार करते हुए भी उनकी कलात्मक त्रुटियों के विषय में कुछ बातें कही गई है। और यह भी कहा गया की ये उस समय के उपन्यास या कहानी की माँग रही हो। सब होते हुए भी प्रेमचंद का महत्व कम नहीं हो सकता।
विविधता भरी लेखनी की लंबी यात्रा का दौर जब रूका तब उनके साथ अनेको कठिनाईयों वाले जीवन का समय धीरे धीरे आगे सरकता रहा वर्ष 1936 मे अचानक पेट में दर्द उठा । खून के दस्त-उल्टियाँ होने लगी। रोग बढ़ता ही गया । बनारस से अपने गाँव लमही जाना चाहते थे पर समय की व चिकित्सा की जरूरत को घ्यान में रख यह संभव न हो सका। अपने मित्र दयानारायण निगम और नरेन्द्र कुमार को बनारस ही बुला लिया। उन्हें आभास हो गया था कहने लगे दुबारा मुलाकात की उम्मीद नहीं है । देर रात तक बातें करते रहे । 07-10-1936 को प्रातः भारत के कर्मठ साहित्यकार प्रेमचंद जी 56 वर्ष, की आयु में अपनी अंतिम सांसे ली और इस जगत से विदा हो गये ।।
उनकी मृत्यु पर एक साहित्यकार ने लिखा था-
“बड़े शौक से सुन रहा था जमाना
तुम्हीं सो गए दास्तां कहते-कहते ”
‘’विश्वास’’नामक कहानी में गाँधी जी के आदर्श को प्रस्तुत किया । (शिक्षाविद—प्रो.रामनारायण जोशी के अनुसार)
इसे कोई गुण माने या दोष, सामयिकता मुंशी जी की कृती मन की प्रधान वृति है । मुंशी जी वर्तमान में जीते है वर्तमान के लिए ही लिखते है। इसलिए कि इन्हें भविष्य की चिंता है ।
आचार्य हजारी प्रसाद व्दिवेदी –‘’प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित अपमानित और उपेक्षित कृषको की आवाज थे’’
उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी को हमारी विनम्र श्रध्दांजलि।
चिरंजीव
लिंगम चिरंजीव राव
म.न.11-1-21/1, कार्जी मार्ग
इच्छापुरम ,श्रीकाकुलम (आन्ध्रप्रदेश)
पिनः532 312 मो.न.8639945892
स्वतंत्र लेखन (संकलन व लेखन)


 राशिफल: जानिए, कैसा रहेगा आपका आज का दिन (27 फ़रवरी 2026)
राशिफल: जानिए, कैसा रहेगा आपका आज का दिन (27 फ़रवरी 2026) रोजगार और व्यापार को बढ़ावा देगा गोंदिया–जबलपुर रेल प्रोजेक्ट
रोजगार और व्यापार को बढ़ावा देगा गोंदिया–जबलपुर रेल प्रोजेक्ट छिंदवाड़ा में युवती से गैंगरेप का आरोप, एक आरोपी गिरफ्तार
छिंदवाड़ा में युवती से गैंगरेप का आरोप, एक आरोपी गिरफ्तार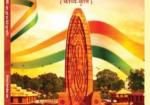 चिरंजीव राव की कृति का विमोचन और डॉ. मौना कौशिक का सम्मान
चिरंजीव राव की कृति का विमोचन और डॉ. मौना कौशिक का सम्मान  45 वर्षीय अधेड़ पर नाबालिग को डरा-धमकाकर बलात्कार करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप
45 वर्षीय अधेड़ पर नाबालिग को डरा-धमकाकर बलात्कार करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप